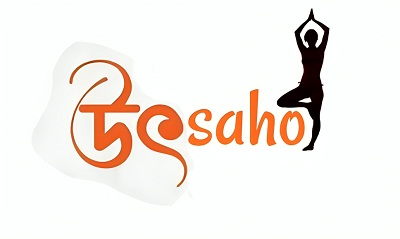साखी , Chapter -7
साखी , Chapter – 7, अभ्यासमाला – प्रश्न और उत्तर
—
1. सही विकल्प का चयन करो –
(क) महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था – सन् 1398 में
(ख) संत कबीरदास के गुरु कौन थे – रामानंद
(ग) कस्तूरी मृग वन-वन में क्या खोजता फिरता है – कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ
(घ) कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है – जो प्रेम का ढाई आखर पढ़ता है
(ङ) कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए – आज
—
2. एक शब्द में उत्तर दो –
(क) श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है
Ans– कीर्तन घोषा
(ख) महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था
Ans– सन् 1518
(ग) कवि के अनुसार प्रेमविहीन शरीर कैसा होता है
Ans– मसान
(घ) कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है
Ans– कुम्हार
(ङ) महात्मा कबीरदास की रचनाएँ किस नाम से प्रसिद्ध हुईं Ans– बीजक
—
3. पूर्ण वाक्य में उत्तर दो –
(क) कबीरदास के पालक पिता-माता कौन थे
Ans– कबीरदास के पालक पिता-माता नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति थे।
(ख) ‘कबीर’ शब्द का अर्थ क्या है
Ans– ‘कबीर’ शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ।
(ग) ‘साखी’ शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है
Ans– ‘साखी’ शब्द संस्कृत के ‘साक्षी’ शब्द से विकसित हुआ है।
(घ) साधु की कौन-सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए
Ans– साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए।
(ङ) डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है
Ans– डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे पर बैठा रहता है।
—
4. अति संक्षिप्त उत्तर दो (लगभग 25 शब्दों में) –
(क) कबीरदास जी की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो
Ans– कबीरदास जी की कविताएँ अपने समय में अत्यंत लोकप्रिय थीं, और आज भी वे उतनी ही लोकप्रिय हैं। श्रीमंत शंकरदेव ने भी ‘कीर्तन घोषा’ में उनका उल्लेख किया है।
(ख) कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे
Ans– कबीरदास जी के आराध्य सर्वव्यापक, निर्गुण और निराकार ‘राम’ थे, जो सृष्टि के प्रत्येक अणु-परमाणु में निवास करते हैं।
(ग) कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है
Ans– उनकी भाषा सरल, सहज और सजीव है। इसे ‘सधुक्कड़ी’ या ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा जाता है। इसमें भावों की स्पष्टता और अलंकारिक सौंदर्य है।
(घ) ‘तेरा साईं तुझ में, ज्यों पुहुपन में बास’ का आशय क्या है
Ans– इसका आशय है कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है, जैसे फूल के भीतर सुगंध समाई रहती है।
(ड.) ‘सत गुरु’ की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है
Ans– कवि ने कहा है कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। वे शिष्य को ज्ञान का नेत्र प्रदान करते हैं और ईश्वर के दर्शन कराते हैं।
(च) ‘अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहै चोट’ का तात्पर्य बताओ
Ans– गुरु बाहर से शिष्य के दोषों को सुधारने के लिए चोट करता है, पर भीतर से स्नेह का सहारा भी देता है।
—
5. संक्षेप में उत्तर दो (लगभग 50 शब्दों में) –
(क) बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है
Ans– कवि कहते हैं कि जब उन्होंने संसार में बुरा व्यक्ति खोजा तो कोई बुरा नहीं मिला। जब अपने मन को देखा तो स्वयं को सबसे बुरा पाया। इससे उन्होंने यह शिक्षा दी कि हमें दूसरों की बुराई खोजने के बजाय अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
(ख) कबीरदास जी ने किसलिए मन का मनका फेरने का उपदेश दिया है
Ans– कबीरदास जी ने कहा कि लोग हाथ की माला फेरते रहे, पर मन का विकार दूर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि माला के दाने छोड़कर मन के विकारों को दूर करो, यही सच्ची साधना है।
(ग) गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं
Ans– गुरु शिष्य को कुम्हार की तरह गढ़ते हैं। जैसे कुम्हार बाहर से चोट करता है पर अंदर से सहारा देता है, वैसे ही गुरु अनुशासन से शिष्य के दोष मिटाते हैं और स्नेह से उसे संभालते हैं।
(घ) कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है
Ans– कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़कर भी कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बनता। जो ‘प्रेम का ढाई आखर’ पढ़ लेता है, वही सच्चा पंडित है। अतः केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का ज्ञान ही सार्थक है।
—
6. सम्यक् उत्तर दो (लगभग 100 शब्दों में) –
(क) संत कबीरदास की जीवन-गाथा पर प्रकाश डालो
Ans–संत कबीरदास का जन्म सन् 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि वे एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जिन्होंने लोकलज्जा के भय से उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने उन्हें पाला। उन्होंने अपने पालक माता-पिता का व्यवसाय अपनाया और जुलाहा बने। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। सन् 1518 में मगहर में उनका देहावसान हुआ। उन्होंने निर्गुण निराकार ‘राम’ की भक्ति की और अपने दोहों के माध्यम से समाज में प्रेम, सद्भाव, ज्ञान और कर्म का संदेश दिया।
(ख) भक्त कवि कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय दो
Ans–कबीरदास जी हिंदी के महान भक्त कवि थे। उनकी वाणी में भक्ति, ज्ञान और मानवता का अद्भुत संगम है। उन्होंने साधारण जन की भाषा में अमूल्य संदेश दिए। उनकी रचनाएँ ‘बीजक’ नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीन भाग हैं। उनकी भाषा ‘सधुक्कड़ी’ कही जाती है, जो सहज और प्रभावशाली है। उन्होंने अपने पदों में प्रेम, आत्मा-परमात्मा, वैराग्य और सत्संग के भावों को सरलता से प्रस्तुत किया। उनके दोहे आज भी जन-जन को प्रेरित करते हैं।
—
7. सप्रसंग व्याख्या करो –
(क) “जाति न पूछो साधु की……………पड़ा रहन दो म्यान।”
संदर्भ – यह साखी संत कबीरदास की रचना है।
प्रसंग – इसमें कवि ने बाहरी रूप से अधिक आंतरिक ज्ञान के महत्व पर बल दिया है।
व्याख्या – कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से मिलते समय उसकी जाति मत पूछो, उसके ज्ञान को पहचानो। जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार से जाना जाता है, म्यान से नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति या रूप से।
(ख) “जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ।”
Ans. संदर्भ – यह साखी संत कबीरदास द्वारा रचित है।
प्रसंग – इसमें कवि ने कर्म और साधना के महत्व पर बल दिया है।
व्याख्या – कवि कहते हैं कि जिन्होंने खोजने का साहस किया, उन्होंने अवश्य पाया, क्योंकि वे गहरे पानी में उतरे। जो डूबने से डर गया, वह किनारे बैठा रह गया। इस प्रकार सफलता पाने के लिए भय त्यागकर प्रयत्न करना आवश्यक है।
(ग) “जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, साँस लेत बिनु प्रान।”
Ans.संदर्भ – यह साखी संत कबीरदास की है।
प्रसंग – इसमें कवि ने प्रेम की महत्ता पर बल दिया है।
व्याख्या – कवि कहते हैं कि जिस शरीर में प्रेम नहीं, वह श्मशान के समान निर्जीव है। जैसे लोहार की धौंकनी हवा तो छोड़ती है, पर उसमें जीवन नहीं होता। प्रेमविहीन मनुष्य भी ऐसा ही है। प्रेम ही जीवन का सार है।
(घ) “काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरि करेगो कब।”
Ans.संदर्भ – यह साखी कबीरदास द्वारा रचित है।
प्रसंग – इसमें समय के मूल्य और कर्मठता का संदेश दिया गया है।
व्याख्या – कवि कहते हैं कि जो काम कल करना है, उसे आज करो, और जो आज का है, उसे अभी करो, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। एक पल में प्रलय हो सकती है, तब अवसर नहीं मिलेगा। यह दोहा मनुष्य को समय का सदुपयोग करने और कर्म करने की प्रेरणा देता है।
—
भाषा एवं व्याकरण-ज्ञान
1. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताओ –
मिरग – मृग
पुहुप – पुष्प
सिष – शिष्य
आखर – अक्षर
मसान – श्मशान
परलय – प्रलय
उपगार – उपकार
तीरथ – तीर्थ
—
2. वाक्यों में प्रयोग करके निम्नलिखित शब्द-युग्मों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो –
मनका – माला का मनका टूट गया।
मन का – मन का भाव शुद्ध होना चाहिए।
अर्थ – मनका का अर्थ है माला का दाना, मन का का अर्थ है हृदय से संबंधित।
करका – ओलों की करका से फसल नष्ट हो गई।
कर का – कर का मनका डारि दे।
अर्थ – करका का अर्थ है ओला, कर का का अर्थ है हाथ से संबंधित।
नलकी – धागे की नलकी खाली हो गई।
नल की – नल की टोटी से पानी टपक रहा था।
अर्थ – नलकी धागा लपेटने की छोटी नली है, नल की का अर्थ नल से संबंधित है।
पीलिया – उसे पीलिया रोग हो गया।
पी लिया – उसने सारा पानी पी लिया।
अर्थ – पीलिया एक रोग है, पी लिया पीने की क्रिया का पूर्ण रूप है।
तुम्हारे – यह काम तुम्हारे लिए आसान है।
तुम हारे – खेल में तुम हारे या जीते।
अर्थ – तुम्हारे का अर्थ है तुम्हारा, तुम हारे का अर्थ है पराजित हुए।
नदी – नदी में बहुत जल था।
न दी – उसने अपनी पुस्तक न दी।
अर्थ – नदी जलधारा है, न दी का अर्थ है नहीं दी।
—
3. निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखो –
महिमा – स्त्रीलिंग
चोट – स्त्रीलिंग
लोचन – पुल्लिंग
तलवार – स्त्रीलिंग
ज्ञान – पुल्लिंग
घट – पुल्लिंग
साँस – स्त्रीलिंग
प्रेम – पुल्लिंग
—
4. निम्नलिखित शब्द-समूहों के लिए एक शब्द लिखो –
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति – कुम्हार
जो जल में डूबकी लगाता हो – गोताखोर
जो लोहे के औजार बनाता है – लोहार
सोने के गहने बनाने वाला कारीगर – सुनार
विविध विषयों का गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति – विद्वान
—
5. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखो –
साईं – प्रभु, ईश्वर, स्वामी
पानी – जल, नीर, अम्बु
पवन – वायु, हवा, समीर
फूल – पुष्प, सुमन, कुसुम
सूर्य – रवि, दिनकर, भानु
गगन – आकाश, नभ, आसमान
धरती – पृथ्वी, धरा, भूमि