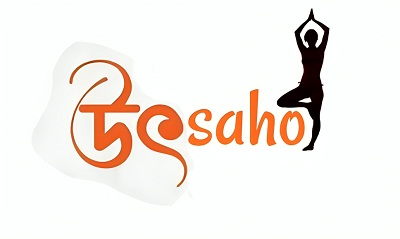6.श्रीमंत शंकरदेव: असम के महापुरुष
भारत की संत परंपरा में श्रीमंत शंकरदेव (1449–1568 ई.) का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वह केवल एक धार्मिक उपदेशक ही नहीं, बल्कि असम की संस्कृति, साहित्य, और कला के महापुरुष थे। पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में, उन्होंने भक्ति आंदोलन की लहर को असम तक पहुँचाया और वहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को एक नई दिशा दी।
शंकरदेव ने ‘एकसरन धर्म’ की स्थापना की, जिसे असम का नव-वैष्णववाद भी कहा जाता है। इस धर्म का मूल सिद्धांत एक ही भगवान (विष्णु या कृष्ण) की शरण लेना और निष्ठापूर्ण भक्ति करना था। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदों को अस्वीकार करते हुए, सभी मनुष्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित ‘सत्र’ (मठ) और ‘नामघर’ (सामुदायिक प्रार्थना घर) आज भी असमिया समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बने हुए हैं।
साहित्य और कला के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ‘कीर्तन घोषा’ है, जो वैष्णव भक्ति गीतों का एक विशाल संग्रह है। इसके अलावा, उन्होंने ‘बोरगीत’ (भक्ति संगीत), ‘अंकिया नाट’ (एक-अंकीय नाटक), और ‘भाओना’ (पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन) जैसी विधाओं को विकसित किया। उन्होंने संस्कृत के बजाय असमिया और ब्रजावली भाषा का उपयोग किया, ताकि उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक आसानी से पहुँच सकें।
संक्षेप में, श्रीमंत शंकरदेव ने असम को न केवल एक धार्मिक पहचान दी, बल्कि उन्होंने वहाँ की भाषा, साहित्य, संगीत और नाट्यकला को भी समृद्ध किया। उनकी शिक्षाएँ आज भी असमिया संस्कृति की रीढ़ बनी हुई हैं और एकता तथा सद्भाव का संदेश देती हैं।
7.असम का हृदय: बिहू उत्सव
बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत त्योहार है, जो यहाँ की संस्कृति, कृषि आधारित जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। यह वास्तव में तीन अलग-अलग उत्सवों का समूह है, जिन्हें साल में तीन बार अलग-अलग मौसमी चरणों में मनाया जाता है: बोहाग बिहू (रोंगाली), काति बिहू (कोंगाली), और माघ बिहू (भोगाली)।
इनमें सबसे प्रमुख है रोंगाली बिहू, जिसे असमिया नव वर्ष की शुरुआत के रूप में अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। ‘रोंगाली’ का अर्थ है ‘आनंद और रंग’। यह उत्सव सात दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना महत्व है। पहले दिन, ‘गोरू बिहू’ पर, किसान अपने मवेशियों को नहलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद मनुष्यों के बीच उत्सव शुरू होता है, जहाँ युवा पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर खुले मैदानों में ऊर्जा से भरा बिहू नृत्य करती हैं। ढोल, पेपा (भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र) और गोगोना जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर पूरा वातावरण गूंज उठता है। लोग एक-दूसरे को प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में पारंपरिक गामोचा (सूती तौलिया) भेंट करते हैं।
दूसरा बिहू, कोंगाली बिहू, अक्टूबर में आता है। ‘कोंगाली’ का अर्थ है निर्धन या सादगी भरा, क्योंकि इस समय धान के भंडार खाली होने लगते हैं और फसलें खेत में होती हैं। यह सादगी का त्योहार है, जिसमें लोग फसल की रक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दौरान आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दीये जलाए जाते हैं।
तीसरा और अंतिम बिहू, भोगाली बिहू, जनवरी में फसल कटाई के बाद आता है। ‘भोगाली’ का अर्थ है भोग या दावत। यह त्योहार भरपूर फसल का जश्न मनाता है, जिसमें पारंपरिक पकवान जैसे ‘पीठा’ और ‘लारू’ बनाए जाते हैं। इस दौरान मेजी (पुआल और बांस का एक अस्थायी ढाँचा) जलाकर अग्नि देवता की पूजा की जाती है और रात भर सामूहिक भोज एवं खेलकूद होते हैं।
बिहू केवल एक पर्व नहीं, बल्कि असमिया लोगों के जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है, जो प्रकृति, समुदाय और एकता का संदेश देता है।
8.असम की प्राकृतिक सुंदरता
भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित असम, वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह राज्य अपनी अतुलनीय हरियाली, विशाल नदियों और समृद्ध वन्यजीवों के कारण ‘पूरब की मणि’ कहलाता है। असम की प्राकृतिक सुंदरता शांत, मनमोहक और शुद्ध है, जो किसी भी आगंतुक को सम्मोहित कर सकती है और उसे शहरी जीवन की भाग-दौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करती है।
असम की सुंदरता का मुख्य आधार यहाँ बहने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है। यह विशाल नदी इस क्षेत्र की जीवनरेखा है और इसे एक भव्य पहचान देती है। मानसून के दौरान जब यह नदी अपने पूरे वेग से बहती है, तो इसका दृश्य अद्भुत और विस्मयकारी होता है। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर फैली उपजाऊ भूमि पर असम के प्रसिद्ध चाय के बागान मौजूद हैं। मीलों तक फैली हरी-भरी चाय की पत्तियाँ एक ऐसी प्राकृतिक कालीन का निर्माण करती हैं, जिसकी सुंदरता और ताजगी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इन बागानों के बीच बसी शांत झीलें और छोटे-छोटे गाँव इसके ग्रामीण सौंदर्य को और भी अधिक निखारते हैं।
यह प्राकृतिक सौंदर्य केवल हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समृद्ध वन्यजीवों में भी निहित है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, जो संकटग्रस्त एक-सींग वाले गैंडे का घर है। यहाँ बाघ, हाथी और विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाती हैं। इसके अलावा, माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक भू-दृश्य मिलकर एक ऐसा अनोखा अनुभव देते हैं जो अविस्मरणीय होता है। दिहांग-दिबांग जैसी पहाड़ियों और घने जंगलों की उपस्थिति असम के परिदृश्य को एक अद्भुत विविधता प्रदान करती है।
संक्षेप में, असम की प्राकृतिक सुंदरता ब्रह्मपुत्र की भव्यता, चाय के बागानों की ताजगी और काजीरंगा के वन्यजीवों का एक मनमोहक मिश्रण है। यह शांति और सौहार्द का प्रतीक है। इस बेजोड़ प्राकृतिक विरासत का संरक्षण हम सबका कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद ले सकें।
9.शिक्षा में खेलों का महत्व
प्रस्तावना
“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।” यह कहावत शिक्षा के संदर्भ में खेलों के महत्व को दर्शाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। खेल इसी विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं।
शारीरिक और मानसिक लाभ
खेल, छात्रों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखकर तंदुरुस्त (fit) बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित खेलकूद से आलस्य दूर होता है और बच्चों में ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक स्तर पर, खेल तनाव को कम करने का सबसे बड़ा माध्यम हैं। यह छात्रों की एकाग्रता (Concentration) और निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making Power) को सुधारता है, जो अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होता है।
सामाजिक और नैतिक विकास
खेलों से प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण लाभ सामाजिक और नैतिक विकास है। टीम गेम्स (Team Games) छात्रों को सहयोग, सद्भाव और टीम भावना सिखाते हैं। वे जीत में विनम्र रहना और हार को gracefully स्वीकार करना सीखते हैं। खेल के मैदान पर उन्हें अनुशासन, समय का पालन, और नेतृत्व (leadership) जैसे जीवन मूल्यों का ज्ञान होता है। वे नियमों का सम्मान करना सीखते हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है।
उपसंहार
शिक्षा और खेल एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है, और खेल हमें यह सिखाते हैं कि उस जीवन को साहस और संघर्ष के साथ कैसे जीना है। स्कूलों और अभिभावकों को खेलों को पढ़ाई जितना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और अनुशासित नागरिक ही एक राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। इसलिए, खेलों को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना अत्यंत आवश्यक है।
10.असम में बाढ़: कारण, प्रभाव और समाधान
प्रस्तावना
असम की पहचान ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी उर्वरक घाटियों से होती है, लेकिन यह नदी प्रतिवर्ष राज्य के लिए भयंकर बाढ़ की त्रासदी भी लाती है। बाढ़ असम के लिए एक मौसमी आपदा बन चुकी है, जो मानसून के महीनों (जून से सितंबर) में जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान करती है। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि कई मानवीय कारकों का भी परिणाम है।
बाढ़ के प्रमुख कारण
असम में बाढ़ का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी का उफान है, जिसका जलस्तर तेज और लगातार बारिश के कारण अचानक बढ़ जाता है। नदी में गाद (silt) जमा होने के कारण इसकी जलधारण क्षमता कम हो गई है, जिससे पानी जल्दी किनारों को तोड़ देता है। इसके अतिरिक्त, नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में वनों की अंधाधुंध कटाई (deforestation) भी एक बड़ा कारण है। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है और नदियों में गाद की मात्रा तेजी से बढ़ती है। दोषपूर्ण तटबंधों और जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था भी इस समस्या को गंभीर बनाती है।
विनाशकारी प्रभाव
बाढ़ का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, और कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। मवेशियों और वन्यजीवों, विशेषकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, का जीवन संकट में पड़ जाता है। बाढ़ के बाद महामारी (जैसे हैजा और टाइफाइड) फैलने का खतरा बढ़ जाता है, और सड़कें तथा पुल टूट जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।
निवारण और समाधान
इस स्थायी समस्या के निवारण के लिए दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं। सबसे पहले, कुशल नदी प्रबंधन (efficient river management) और उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों (forecasting systems) को लागू करना होगा। तटबंधों की नियमित मरम्मत और मजबूती आवश्यक है। इसके साथ ही, जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण (Afforestation) को बढ़ावा देना और गाद निकालने (dredging) की परियोजनाएं शुरू करना भी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से ही असम के लोगों को इस वार्षिक त्रासदी से बचाया जा सकता है।